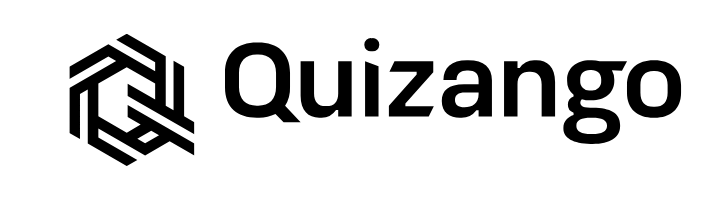परिचय
भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में ग्रामीण क्षेत्र देश की आत्मा हैं। यहां की बड़ी जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि या असंगठित श्रम पर निर्भर है। ऐसे में गरीबी, बेरोजगारी और मौसमी मजदूरी बड़ी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं से निपटने और हर ग्रामीण परिवार को काम का अधिकार देने के उद्देश्य से सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया — मनरेगा (MGNREGA)।
मनरेगा न केवल भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, बल्कि यह कानूनी रूप से गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने वाला एकमात्र कार्यक्रम भी है। इस लेख में हम मनरेगा के सभी पहलुओं, इसके उद्देश्य, कार्य प्रणाली, उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
मनरेगा क्या है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे सामान्यतः मनरेगा कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 2005 में पारित किया गया एक कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार (शारीरिक श्रम आधारित कार्य) प्रदान किया जाता है।
यह कार्य ग्रामीण विकास से जुड़े होते हैं, जैसे — सड़क निर्माण, जल संरक्षण, सिंचाई, पौधारोपण, तालाब की सफाई आदि।
मनरेगा का इतिहास और पृष्ठभूमि
- 2005 में संसद में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया।
- प्रारंभ में इसे 200 जिलों में शुरू किया गया था और फिर 2008 तक पूरे भारत में विस्तारित कर दिया गया।
- यह कानून ‘रोजगार का अधिकार’ देने वाला पहला प्रयास था।
- इसका नाम बाद में महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया।
मनरेगा का उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य:
- ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना।
- ग्रामीण परिवारों को आजीविका की गारंटी देना।
- पर्यावरण संरक्षण और स्थायी ग्रामीण विकास कार्य करना।
- सामाजिक समावेशन और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना।
मनरेगा की प्रमुख विशेषताएँ
1. कानूनी अधिकार
मनरेगा के अंतर्गत रोजगार कानूनी अधिकार है। यदि सरकार 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं देती, तो मजदूरों को भत्ता (Unemployment Allowance) देना पड़ता है।
2. न्यूनतम 100 दिन रोजगार
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है।
3. महिला भागीदारी
कम से कम 33% कार्य महिला श्रमिकों को आवंटित किया जाता है, जिससे महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलती है।
4. स्थानीय और मांग आधारित रोजगार
रोजगार की मांग ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, जिससे यह नीचे से ऊपर की योजना बन जाती है।
5. पारदर्शिता और जन निगरानी
कार्य की निगरानी में सामुदायिक भागीदारी, सोशल ऑडिट और MIS सिस्टम की मदद से पारदर्शिता बनाए रखी जाती है।
मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले कार्य
1. जल संरक्षण एवं संरक्षण कार्य
- तालाबों की खुदाई
- जलाशयों का निर्माण
- चेक डैम बनाना
2. सिंचाई और कृषि कार्य
- खेत की मेड़बंदी
- सिंचाई चैनल
- वृक्षारोपण
3. सड़क निर्माण
- कच्ची सड़कों का निर्माण
- पगडंडियों का सुधार
4. पंचायत भवन, स्कूल परिसर विकास
- सामुदायिक भवनों का निर्माण
- आंगनवाड़ी केंद्रों का सुधार
मनरेगा में पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया
1. पंजीकरण
- इच्छुक ग्रामीण परिवार को ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन देना होता है।
- जॉब कार्ड (Job Card) प्राप्त करना आवश्यक है।
2. रोजगार की मांग
- परिवार के कोई भी सदस्य जॉब कार्ड दिखाकर रोजगार की मांग कर सकता है।
- पंचायत को 15 दिनों के अंदर कार्य देना अनिवार्य है।
3. कार्य स्थल पर सुविधाएं
- पीने का पानी, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था
- बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच
मनरेगा का वित्त पोषण
- 75% खर्च केंद्र सरकार वहन करती है।
- 25% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- मजदूरी का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से होता है।
मनरेगा की उपलब्धियाँ
1. रोजगार में वृद्धि
हर साल 5 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। महामारी जैसे संकट काल में यह योजना आजीविका का आधार बनी रही।
2. महिला सशक्तिकरण
मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक रही है, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है।
3. पर्यावरण संरक्षण
जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूमि सुधार जैसे कार्यों से पर्यावरणीय संतुलन में योगदान मिला।
4. ग्रामीण विकास में सहयोग
सड़कों, पुल, सिंचाई व्यवस्था और सामुदायिक संरचनाओं के निर्माण से ग्रामों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ।
मनरेगा से संबंधित समस्याएं और चुनौतियाँ
1. भुगतान में देरी
अक्सर मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं होता, जिससे असंतोष उत्पन्न होता है।
2. भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका
कुछ क्षेत्रों में फर्जी जॉब कार्ड, घोषित कार्यों में घपला, और बिचौलियों का हस्तक्षेप देखा गया है।
3. तकनीकी अड़चनें
DBT और MIS सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण मजदूरी नहीं पहुंचती।
4. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता
कुछ कार्यों की गुणवत्ता कमजोर होती है, जिससे स्थायित्व और प्रभाव पर असर पड़ता है।
भविष्य की दिशा और सुझाव
1. डिजिटल निगरानी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
MIS पोर्टल, मोबाइल ऐप और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) की मदद से निगरानी को प्रभावी बनाया जाए।
2. महिला केंद्रित कार्यों को प्राथमिकता
महिलाओं की सुविधा के अनुसार गृह निकट कार्य, पौधारोपण, शिक्षा केंद्र निर्माण आदि को प्राथमिकता दी जाए।
3. स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना
ग्राम सभा, पंचायत, स्वयंसेवी संगठन को योजना में अधिक सक्रिय भागीदारी मिलनी चाहिए।
4. रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाना
100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन तक रोजगार देने पर विचार किया जाए, विशेष रूप से आदिवासी और गरीब जिलों में।
महत्वपूर्ण कीवर्ड्स (Keywords):
- मनरेगा क्या है
- महात्मा गांधी रोजगार योजना
- जॉब कार्ड कैसे बनवाएं
- ग्रामीण रोजगार योजना
- MGNREGA रजिस्ट्रेशन
- मनरेगा में मजदूरी
- DBT भुगतान मनरेगा
- महिला भागीदारी मनरेगा
- जल संरक्षण योजना ग्रामीण भारत
- ग्राम पंचायत रोजगार योजना
निष्कर्ष
मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और पर्यावरण संरक्षण तीनों को एक साथ साधा है। यह केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का आधार है।
यदि इस योजना को पारदर्शिता, दक्षता और सहभागिता के साथ लागू किया जाए, तो यह भारत को ग्रामोन्मुख और समावेशी विकास की दिशा में ले जाने वाला एक सशक्त माध्यम बन सकता है।